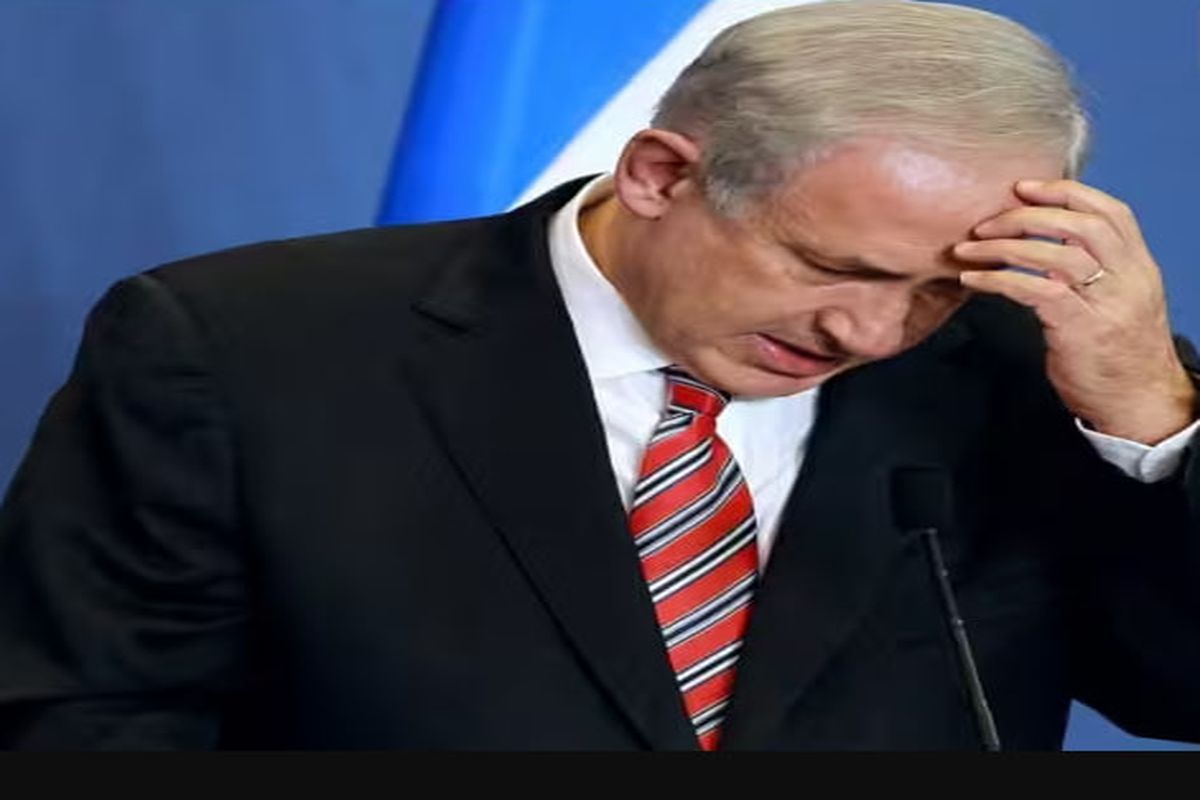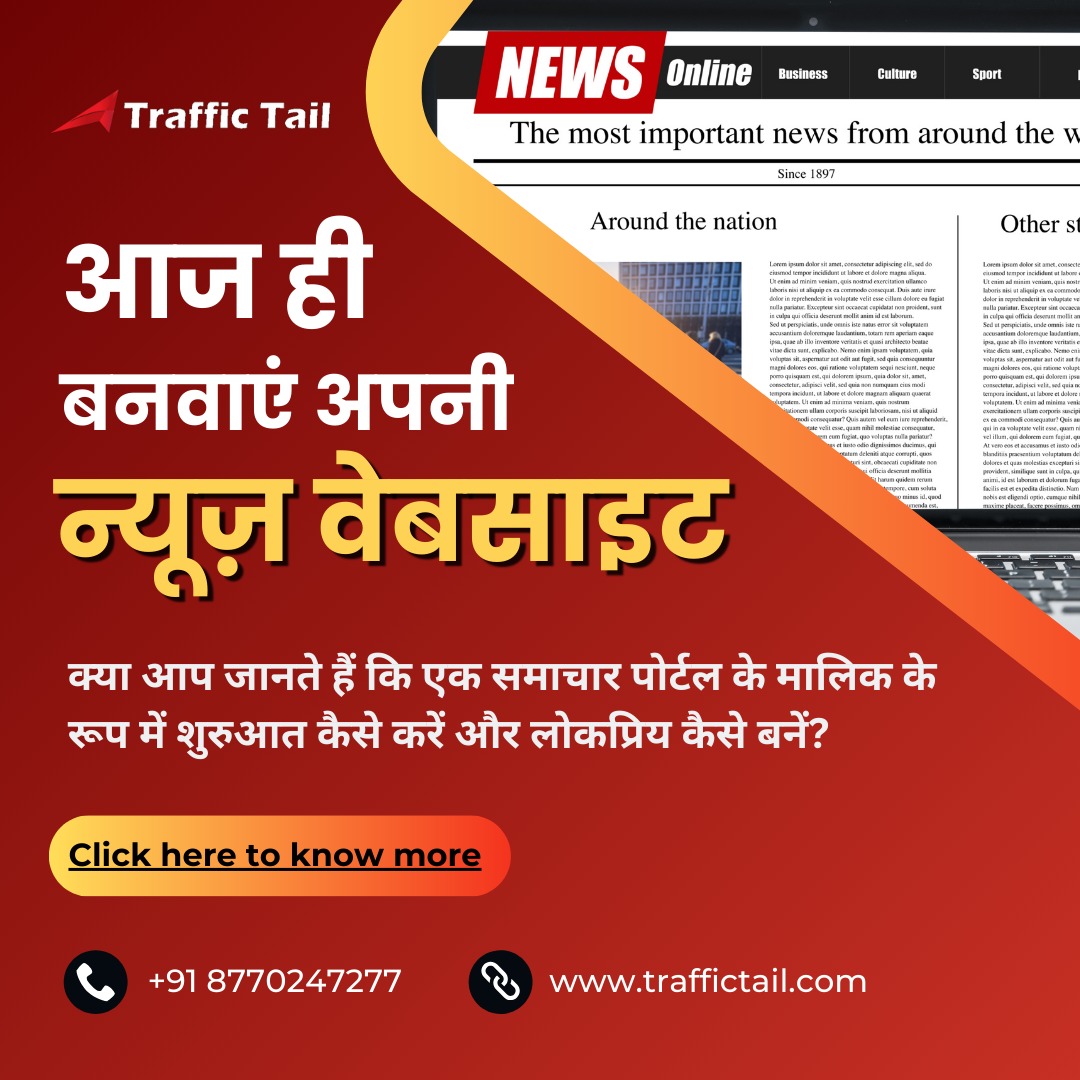नई दिल्ली. Ajab-Gajab Station Of India: भारत में रेलवे सिर्फ एक परिवहन व्यवस्था नहीं, बल्कि देश की सामाजिक-आर्थिक रेखा है। हर दिन लाखों लोग ट्रेनों के ज़रिये काम पर जाते हैं, रिश्तेदारी निभाते हैं, सपने पूरे करते हैं। 1853 में पहली ट्रेन चलने के बाद रेलवे का नेटवर्क आज विश्व के सबसे बड़े नेटवर्कों में शामिल है। जहां एक ओर बुलेट ट्रेन, वंदे भारत और सेमी-हाईस्पीड रेल जैसी आधुनिक परियोजनाएं चर्चा में हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़ोन में एक ऐसा स्टेशन भी है जो विकास की इस दौड़ में पीछे छूट गया, मगर पूरी ताकत से वापस आने की जिद में है।
दयालपुर स्टेशन: वो जगह जहां हर टिकट में बसी है उम्मीद
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है दयालपुर रेलवे स्टेशन, जो भले एक छोटा-सा स्टेशन है, लेकिन इसकी कहानी पूरे भारतीय रेलवे के सिस्टम को आईना दिखा सकती है। यह वो स्टेशन है जहाँ हर दिन टिकट खरीदी जाती है, मगर कोई ट्रेन की यात्रा नहीं करता। यह कोई किस्सा नहीं, बल्कि हकीकत है। एक सच्ची मिसाल, जो दर्शाती है कि आम आदमी जब अपनी जिद पर उतर आए, तो व्यवस्था को भी झुकना पड़ता है।
इतिहास में दर्ज हुआ था जब नेहरू ने किया उद्घाटन
1954 का साल, भारत आज़ाद हुए कुछ ही साल बीते थे। देश निर्माण की प्रक्रिया जोरों पर थी। उसी दौर में, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दयालपुर स्टेशन का उद्घाटन किया था। उस समय यह स्टेशन ग्रामीण इलाकों को शहरों से जोडऩे का एक महत्वपूर्ण जरिया था। यहां कई ट्रेनें रुकती थीं, बाजार की रौनक होती थी, यात्री ट्रेन पकड़ते और लौटते थे। दयालपुर तब सिर्फ एक नाम नहीं था-वह लोगों की जरूरत और पहचान था।
धीरे-धीरे स्टेशन की रफ्तार थमी, और 2006 में लगा ताला
समय बदला। जैसे-जैसे सडक़ यातायात बढ़ा, ग्रामीण परिवहन के निजी विकल्प बढ़े, वैसे-वैसे स्टेशन की उपयोगिता कम होती गई। रेलवे विभाग ने देखा कि स्टेशन से हर दिन औसतन 50 से भी कम टिकट बिक रहे हैं। रेलवे के नियमों के अनुसार, अगर किसी स्टेशन से रोज़ इतनी कम टिकट बिकें तो वह स्टेशन घाटे में माना जाता है और बंद करने योग्य हो जाता है और ऐसा ही हुआ-2006 में रेलवे ने दयालपुर स्टेशन को बंद कर दिया।
गांववालों के लिए यह एक सदमा था
दयालपुर और आसपास के गांवों के लोगों के लिए यह सिर्फ स्टेशन बंद होना नहीं था – यह उनके जीवन की एक धुरी टूटने जैसा था। गांव के बुज़ुर्गों के लिए यह गर्व का प्रतीक था कि उनके यहां नेहरू जी आए थे, स्टेशन खोला था। जब स्टेशन बंद हुआ, तो वहां सिर्फ वीरानी बची। खाली प्लेटफॉर्म, उखड़ते खंभे, जंग लगे बोर्ड और एक भारी-भरकम ताला। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती,बल्कि यहीं से शुरू होती है एक ऐसा अध्याय, जिसे आज भी लोग च्च्दयालपुर की जिदज्ज् कहते हैं।
स्थानीय जनता ने किया संघर्ष-स्टेशन दोबारा चाहिए
गांव के लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया, ज्ञापन दिए, कई बार डीआरएम ऑफिस के चक्कर लगाए। पंचायतों में प्रस्ताव पारित हुए, स्थानीय नेताओं ने आवाज़ उठाई। एक दशक से ज़्यादा संघर्ष के बाद 2020 में रेलवे ने स्टेशन को दोबारा खोल दिया। यह बड़ी जीत थी। लेकिन इस जीत में एक ट्विस्ट था-स्टेशन खुला जरूर, लेकिन सुविधाएं नहीं आईं। ट्रेनें नहीं बढ़ीं, स्टाफ नहीं आया, टिकट काउंटर तो खुला पर कर्मचारी सीमित।
अब रोज़ लोग टिकट खरीदते हैं… मगर ट्रेन में चढ़ते नहीं!
दयालपुर स्टेशन पर अब केवल एक ट्रेन रुकती है- प्रयागराज-आलवर पैसेंजर। वो भी सिर्फ दिन के एक तय वक्त पर। लेकिन यहां के लोगों ने एक अनोखा रास्ता निकाला- वे रोज टिकट खरीदने लगे, चाहे उन्हें कहीं जाना हो या नहीं। बस एक ही मकसद कि रेलवे को लगे कि यहां मांग है, स्टेशन चालू रहना चाहिए। रिपोट्र्स के मुताबिक, हर महीने यहां 700 रुपये तक की टिकटें बिकती हैं-वो भी बिना यात्रा के! कई बार लोग टिकट खरीदकर फाड़ देते हैं, लेकिन टिकट काउंटर से रसीद ज़रूर लेते हैं, क्योंकि आंकड़ों में स्टेशन को चालू दिखाना जरूरी है।
यह सिर्फ टिकट नहीं-आंदोलन है, प्रतीक है
दयालपुर में टिकट खरीदना एक आंदोलन बन चुका है। यह स्थानीय लोगों की उस मानसिकता को दर्शाता है जिसमें वे अपनी ज़मीन, अपने संसाधन, और अपनी विरासत के लिए जूझते हैं। उनका मानना है कि अगर आज हम चुप हो गए, तो कल हमारे बच्चे पूछेंगे-क्या कभी यहां ट्रेन आती थी?
एक ट्रेन, एक उम्मीद-सुविधाएं अब भी नदारद
आज भी दयालपुर स्टेशन पर कोई छत नहीं है, न बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, न ही शौचालय या पीने का पानी। बोर्ड जर्जर हो चुका है, और लाइटिंग की हालत खराब है। लेकिन लोग कहते हैं कि च्च्हम सरकार से कोई महल नहीं मांग रहे, बस चाहते हैं कि ट्रेनें रुके, सुविधा हो और स्टेशन जीवित रहे।ज्ज्
रेलवे की स्थिति-च्न लाभकारी, न प्राथमिकता में
रेलवे अधिकारियों की मानें तो दयालपुर जैसे स्टेशनों को सक्रिय रखना आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है। रेल मंत्रालय अधिकतर निवेश वहीं करता है जहां यात्रियों की संख्या ज़्यादा हो या उद्योगिक महत्त्व हो। दयालपुर जैसे स्टेशन ‘लो ट्रैफिक हॉल्ट’ श्रेणी में आते हैं, जिन्हें सीमित संसाधनों में ही चलाना होता है। लेकिन ये तर्क स्थानीय जनता के जोश के आगे फीके पड़ जाते हैं।
आगे की राह क्या? क्या कभी यह स्टेशन फिर गुलजार होगा?
दयालपुर की कहानी से यह सवाल उठता है- क्या ऐसे स्टेशनों को मरने दिया जाए? या लोगों की भावना को देखते हुए उन्हें संरक्षित किया जाए? विशेषज्ञों का सुझाव है कि रेलवे को कम लागत वाले ऑटोमेटेड टिकट मशीन, सोलर लाइटिंग, और डिजिटल हॉल्ट स्टेशन मॉडल पर काम करना चाहिए। इससे छोटे स्टेशनों को बंद करने की नौबत नहीं आएगी और स्थानीय परिवहन को जीवन मिलेगा।
दयालपुर की कहानी-एक उदाहरण, एक प्रेरणा
दयालपुर रेलवे स्टेशन आज भले एक उपेक्षित जगह हो, लेकिन यह उन लाखों गांवों की आवाज़ है जो विकास के नक्शे से गायब हैं।
यह कहानी हमें बताती है कि:
- जनता अगर ठान ले, तो व्यवस्था को जवाब देना ही पड़ता है।
- आवाज सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं, ज़मीन पर खड़े होकर उठानी होती है।
- और सबसे अहम-टिकट कभी-कभी सिर्फ मंज़िल के लिए नहीं, आंदोलन के लिए भी खरीदी जाती है।
जहां ट्रेन न रुके, वहां उम्मीदें भी ठहर जाएं-ऐसा दयालपुर नहीं मानता
दयालपुर हमें यह सिखाता है कि हार सिर्फ आंकड़ों में होती है, जज़्बे में नहीं। वहां रोज टिकट बिकता है – एक प्रतीक बनकर। कोई सफर नहीं करता, फिर भी आंदोलन चलता है। और यही आंदोलन, एक दिन शायद ट्रेन को फिर पूरी रफ्तार से इस स्टेशन पर लाएगा- छुक-छुक करती उम्मीदों के साथ।